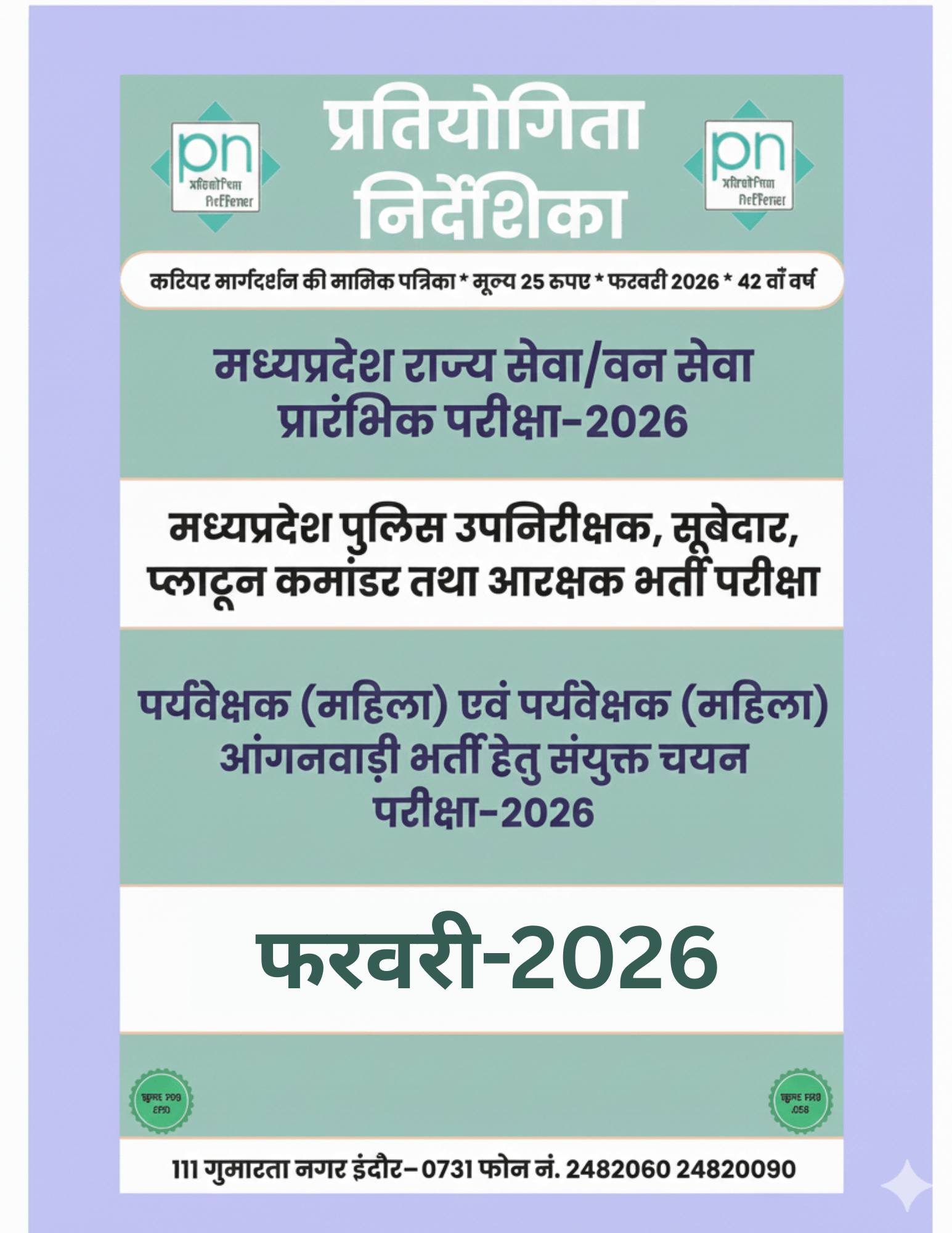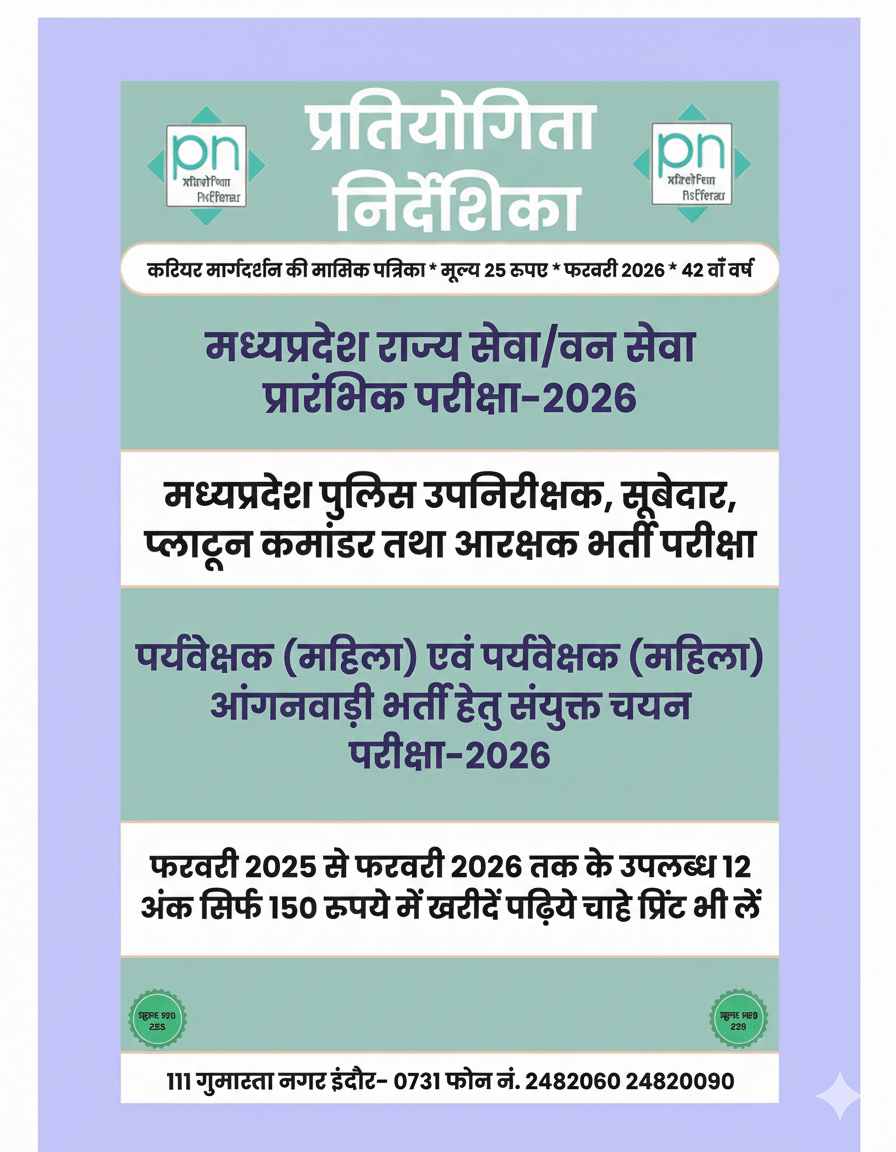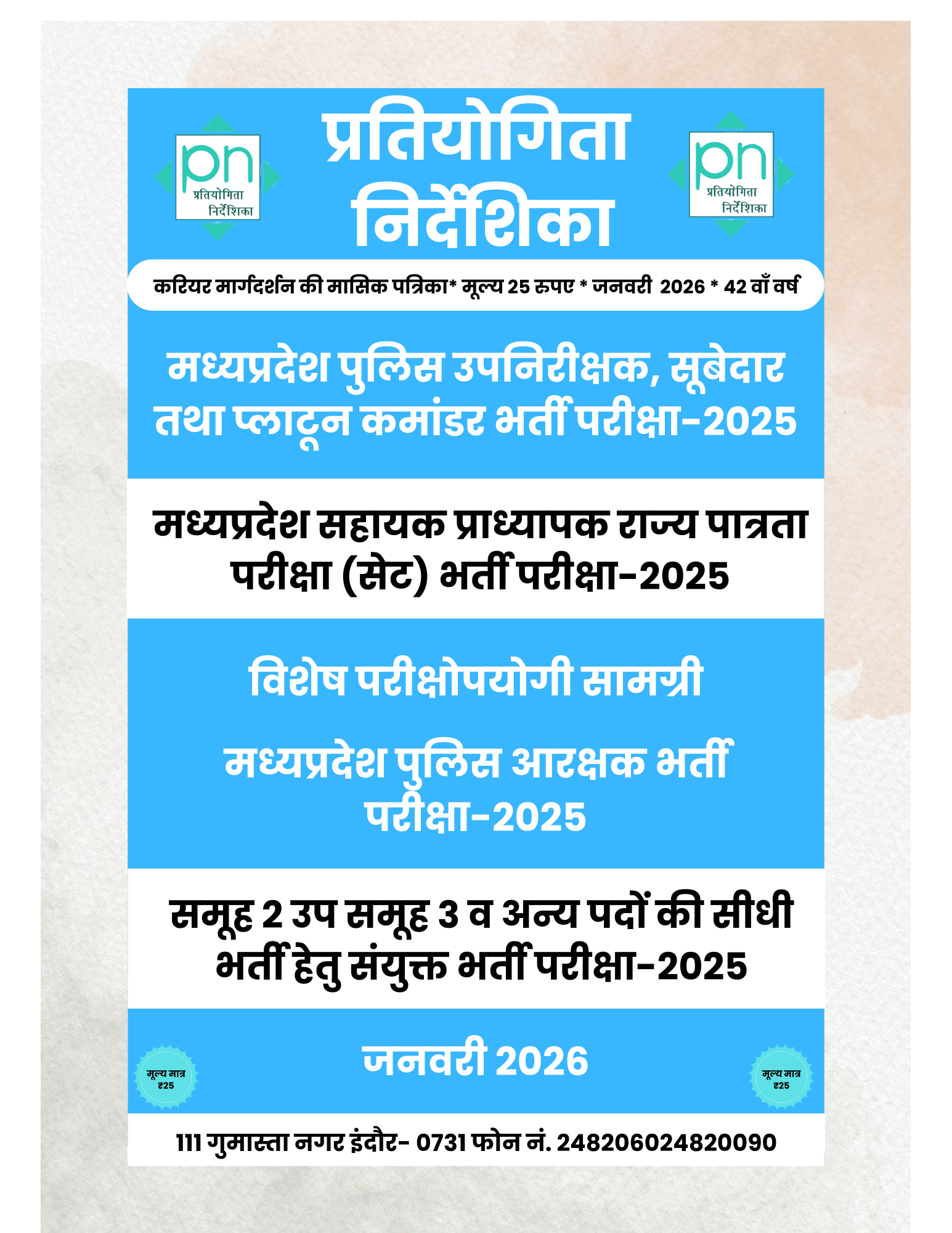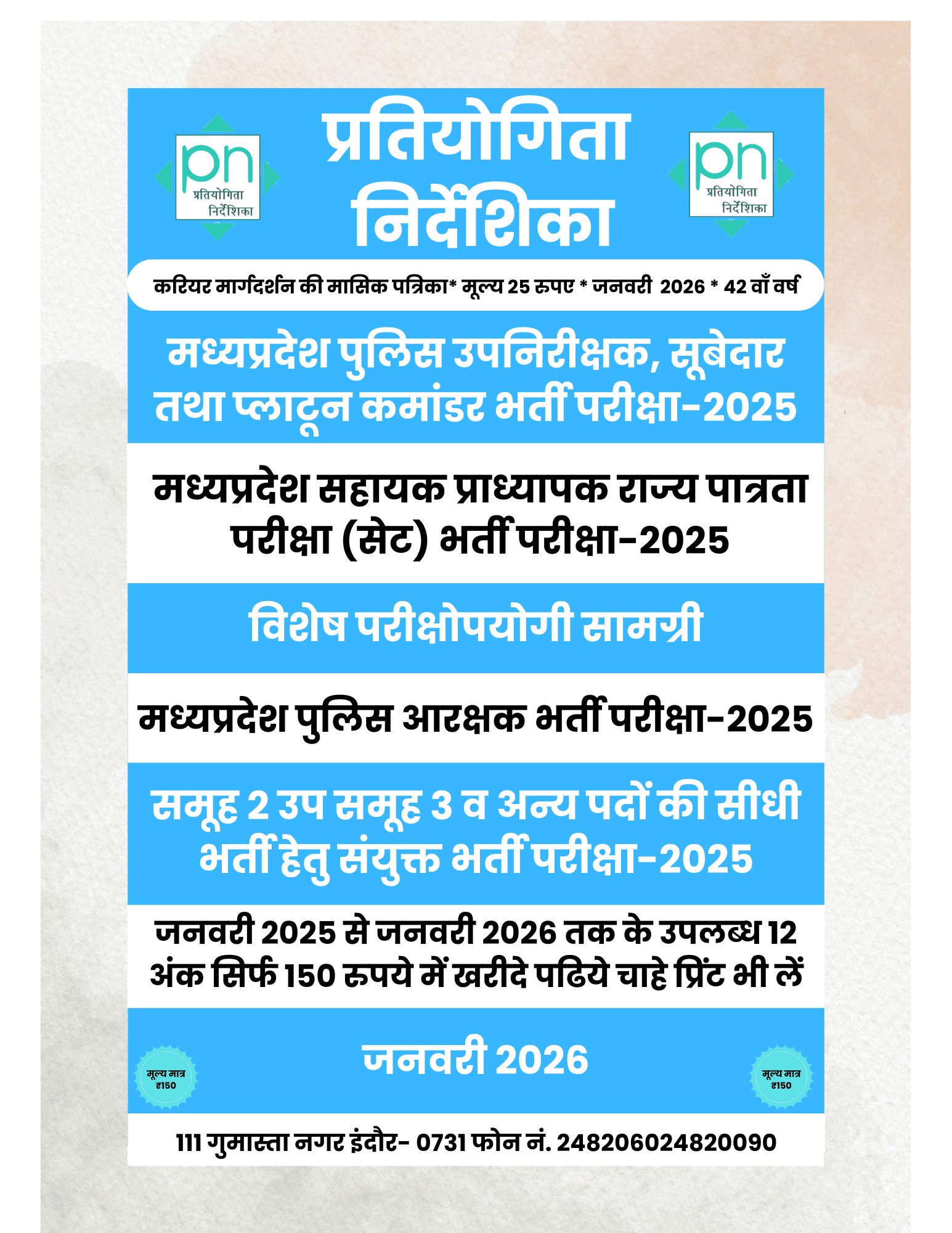मैं सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कॅरियर बनाना चाहता हूँ। कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें।
वर्तमान समय में हमारे देश में बुनियादी ढाँचे का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। बड़े शहरों ही नहीं छोटे शहरों एवं कस्बों में भी निर्माण उद्योग के क्षेत्र में नई चमक दिखाई दे रही है। बुनियादी ढांचे के विकास और तेज निर्माण कार्यों ने सिविल इंजीनियरिंग का महत्व बढ़ाया है। रियल एस्टेट के अलावा भी कई सारे कंस्ट्रक्शन कार्य जैसे पुल का निर्माण, सडक़ों की रूपरेखा, एयरपोर्ट निर्माण, सीवेज सिस्टम निर्माण आदि कार्य को अपने कौशल द्वारा आगे ले जाने का कार्य सिविल इंजीनियर कर रहे हैं। नैस्कॉम की एक नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक इस समय माँग की अपेक्षा देश में सिविल इंजीनियरों की संख्या बहुत कम है जबकि 2020 के अंत तक देश में करीब एक लाख सिविल इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ेगी। गौरतलब है कि जब भी कोई निर्माण योजना बनती है तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग, डिजाइनिंग तथा स्ट्रक्चरल कार्य से लेकर अनुसंधान एवं सेल्यूशन तैयार करने का कार्य किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया सिविल इंजीनियरिंग कहलाती है। यह कार्य किसी सामान्य व्यक्ति से न कराकर प्रोफेशनल लोगों से ही कराया जाता है, जो कि सिविल इंजीनियर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों को किसी प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन या मेंटिनेंस का कार्य करना होता है। साथ ही इस कार्य के लिए उनकी जिम्मेदारी भी तय होती है। ये स्थानीय निकाय के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं तथा उन्हें स्वयं को कार्यक्षेत्र में संबंधित निकाय के सामने सिद्ध भी करना होता है। किसी भी प्रोजेक्ट एवं परियोजना की लागत, कार्यसूची, क्लाइंट्स एवं कांट्रेक्टरों से संपर्क आदि कार्य भी सिविल इंजीनियरों को ही करनेे होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का कार्यक्षेत्र बहुत फैला हुआ है। जरूरत इस बात की है कि छात्र अपनी रूचि के अनुसार ही क्षेत्र का चयन करे। इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आदि हैं। सिविल इंजीनियरों की देश के साथ-साथ विदेशों में भी कार्य की संभावना बढ़ती जा रही है। प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों एवं कंस्ट्रक्शन कंपनियों के भारत में आने से यहाँ भी इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ प्रबल हो गई हैं। सिविल इंजीनियर बनने के लिए पहले छात्र को बीटेक या बीई करना होती है, जो कि बारहवीं (भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा गणित) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही संभव होती है। दसवीं के बाद पोलिटेक्निक के जरिए भी सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया जा सकता है। जो डिप्लोमा श्रेणी में आता है। सिविल इंजीनियरिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु प्रवेश परीक्षा में चयनित होना होता है। प्रतिष्ठिïत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) तथा प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों से सिविल इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम करने हेतु आईआईटी मेन्स/ एडवान्स प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना होती है। जबकि प्रदेश के पोलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश के लिए पीपीटी परीक्षा में सफल होना होता है। सिविल इंजीनियर का पेशा काफी जिम्मेदारी वाला एवं सम्मानजनक होता है। बिना रचनात्मक कौशल के इसमें सफलता मिलना या आगे कदम बढ़ाना मुश्किल है। नित नए प्रोजेक्ट एवं चुनौतियों के रूप में काम करना पड़ता है। एक सिविल इंजीनियर को बहुत ही शार्प, एनालिटिकल एवं प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसके साथ-साथ संवाद कौशल का गुण भी उसके भीतर होना चाहिए। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का कार्य एक प्रकार का टीमवर्क है जिसमें लोगों से मेलजोल भी रखना पड़ता है। इसके अलावा एक इंजीनियर में दबाव में भी बेहतर कार्य करने, समस्या का तत्काल हल निकालने तथा संगठनात्मक गुण का होना नितांत आवश्यक है जबकि तकनीकी ज्ञान, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े कम्प्यूटर के प्रमुख सॉफ्टवेयरों की जानकारी, बिल्डिंग एवं उसके सुरक्षा संबंधी अहम उपाय, ड्राइंग, लोकल अथॉरिटी एवं सरकारी संगठनों से बेहतर तालमेल, प्लानिंग का कौशल आदि का ज्ञान सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। एक सिविल इंजीनियर को सरकारी संस्थानों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की इंडस्ट्रीज, शोध एवïं शैक्षिक संस्थान आदि में काम करने का अवसर प्राप्त होता है। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आज इसमें संभावनाएँ काफी तेजी से बढ़ी हैं। इसका प्रमुख कारण रियल एस्टेट में आई क्रांति ही है। जिसके चलते हर जगह बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट आदि का निर्माण किया जा रहा है। सिविल इंजीनियर किसी भी यूनिट को रिपेयरिंग, मेंटिनेंस से लेकर कंस्ट्रक्शन तक का कार्य करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बीई करने के बाद रोड प्रोजेक्ट, बिल्डिंग वक्र्स, कन्सल्टेंसी फर्म, क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज या हाउसिंग सोसायटी में काम के अवसर मिलते हैं। केंद्र एवं प्रदेश सरकार के संस्थानों में सिविल इंजीनियरों के लिए काम के बहुत अवसर मौजूद हैं। इसके अलावा रेलवे, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, कंसल्टेंसी में भी रोजगार की ढेरों संभावनाएँ हैं। अनुभव बढऩे के साथ सिविल इंजीनियर चाहे तो अपनी स्वयं की कंसल्टेंसी सर्विस भी खोल सकता है। सरकारी संस्थानों में सिविल इंजीनियर को मिलने वाला वेतन ज्यादातर केंद्र अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग पर निर्भर करता है जबकि प्राइवेट कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला पैकेज उम्मीदवार की योग्यता एवं अनुभव से जुड़ा होता है।